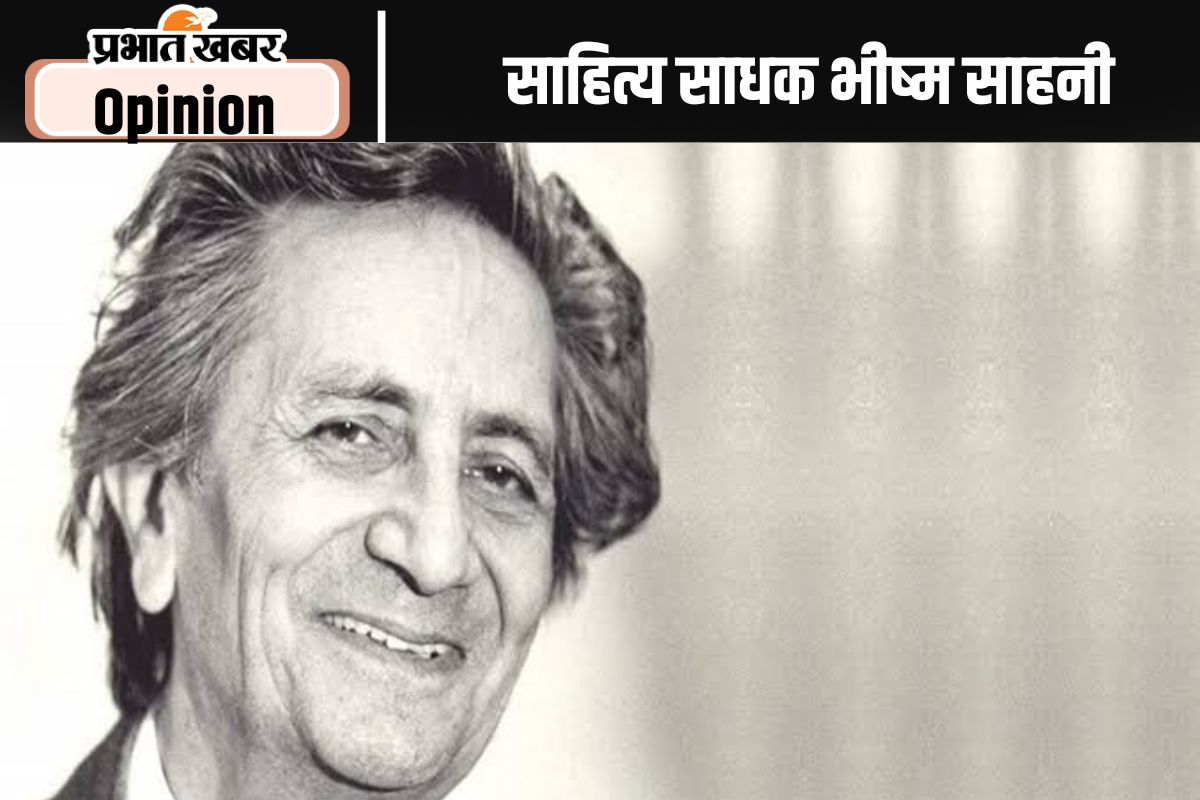Bhisham Sahni : हिंदी के साहित्य साधकों में 1947 में घटित हुई देश के विभाजन की विभीषिका पर कलम चलाने वालों की- यशपाल, राही मासूम रजा और कमलेश्वर से लेकर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ और कृष्णा सोबती आदि तक की- एक खासी लंबी शृंखला है. परंतु इसके चलते हुई जन-धन की हानि और दर-ब-दर होने की पीड़ा को जिस तरह भीष्म साहनी ने महसूस किया है, शायद ही किसी और ने किया हो. हालांकि इसे लेकर अपना लोकप्रिय उपन्यास ‘तमस’ उन्होंने विभाजन के कई दशकों बाद, 1970 में महाराष्ट्र के जलगांव व भिवंडी आदि में हुए दंगों को देखने के बाद लिखा, जो 1972 में प्रकाशित हुआ. पर इसने उस विभीषिका के इतने पहलुओं को ऐसे-ऐसे कोण से उजागर किया कि उसे उनके प्रभूत पूर्ववर्ती लेखन को अपने पीछे कर देने में कोई दिक्कत नहीं हुई. फिर तो यह उपन्यास उनके नाम से ऐसा जुड़ गया कि वे सबसे अधिक इसी के लिए जाने जाने लगे.
वर्ष 1975 में उन्हें साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इसी के लिए मिला. अलबत्ता, उनके संपूर्ण योगदान के लिए 1969 में उन्हें ‘पद्मश्री’ और 1998 में ‘पद्मभूषण’ से नवाजा गया. कहा जाता है कि वे ‘तमस’ को ऐसे रूप में इसलिए लिख पाये कि जलगांव व भिवंडी आदि के दंगों ने उनकी जन्मस्थली रावलपिंडी (जहां वे आठ अगस्त, 1915 को पैदा हुए थे और जो अब पाकिस्तान में है) की उनके बचपन व छुटपन की अनेक त्रासद यादें ताजा कर दी थीं.
एक आलोचक के शब्द उधार लेकर कहें तो उनके इस उपन्यास ने अपने पाठकों को साफ-साफ बताया कि कैसे किसी बहुभाषी, बहुधर्मी समाज में नाना प्रकार के कल्पित डर, अफवाहें और असुरक्षा की गहरी भावनाएं किसी एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों से डरने और घृणा करने के लिए उकसा देती हैं. इस कदर कि उकसावे से पैदा हुई कटुता के बीच उनकी मानवता कहीं खो जाती है. एक अन्य आलोचक के अनुसार, भीष्म साहनी ने अपने दिल की आवाज पर लेखक बनने का निर्णय कर कलम थामी, तो जल्दी ही उसे अवाम की आवाज बनाने में सफल रहे थे. जहां तक विभाजन की बात है, उसे लेकर उन्होंने ‘तमस’ उपन्यास के अतिरिक्त ‘अमृतसर आ गया है’, ‘पाली’ और ‘निमित्त’ जैसी मार्मिक कहानियां भी लिखी हैं.
आज की तारीख में उनके साहित्य का कोई भी सहृदय पाठक यह देखकर विस्मित हो जाता है कि विभाजन के जाये नाना प्रकार के दर्दों के लंबे दौर से गुजरने के बावजूद वे अपने उपन्यासों, कहानियों और नाटकों में प्रायः आशा, विश्वास व सकारात्मकता से भरे हुए नजर आते हैं और यह सकारात्मकता उनके साहित्य में बखूबी अभिव्यक्त होती है. अपने एक बहुचर्चित साक्षात्कार में उन्होंने कहा है, ‘जीवन बड़ा पेचीदा होता है. न वह किसी जगह थमता है और न स्थायी होता है. हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ वक्त भी बदलता रहता है और जो शक्तियां उसे बदलती हैं, वे भी एक जैसी नहीं रहतीं. इसलिए आज अगर नकारात्मक पहलू जोर पर है, तो उन्हें लेकर मायूस होने की कतई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कल कहीं ज्यादा सकारात्मक पहलू आगे आ जाये.’ उनका यह भी मानना था कि किसी समाज में अच्छा या बुरा, जो कुछ भी होता है, उसके लिए उस समाज के सारे लोग जिम्मेदार होते हैं और वे उसकी जिम्मेदारी किसी और पर थोपकर स्वयं उससे नहीं बच सकते. वे कहते थे कि ‘किसी भी लेखक के लिए साहित्य सृजन उन खो गये रास्तों की तलाश का उपक्रम होना चाहिए, जिन्हें हमने मानवता की चूकों के कारण खोया.’ उन्हीं के शब्दों में कहें, ‘तो हर बीता कल हमें चेताता है कि हमें उन चूकों से सबक लेकर अपने आज को संभालना है, ताकि अपने कल को बचा सकें.’
उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, लेकिन शिक्षा-दीक्षा हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में हुई. उनका रूसी समेत कई विदेशी भाषाओं पर भी अधिकार था. हिंदी का सौभाग्य कि उन्होंने इन सारी भाषाओं पर उसे तरजीह दी और उसे अपने सृजन की भाषा के रूप में चुना. उनकी पहली कहानी ‘अबला’ उनके कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, दूसरी ‘हंस’ में और इसके बाद वे बहुविध सृजन में रत हुए, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, निबंधों और बाल साहित्य के सृजन के अलावा शिक्षण, अनुवाद और अभिनय के क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमाये थे. वर्ष 1965 से 1967 तक उन्होंने कहानियों की अपने समय की बहुचर्चित पत्रिका ‘नयी कहानियां’ का संपादन भी किया था. उनके लिखे ‘हानूश’ और ‘कबिरा खड़ा बाजार में’ जैसे नाटक हिंदी थिएटर के दुर्दिन में भी उसके लिए प्रासंगिक बने हुए हैं. वर्ष 2003 की 11 जुलाई को, दुनिया को अलविदा कहने से कुछ ही समय पहले ‘आज के अतीत’ शीर्षक से प्रकाशित अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों को बेलाग-लपेट प्रस्तुत किया है. इस आत्मकथा को उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करने के लिए भी जाना जाता है.