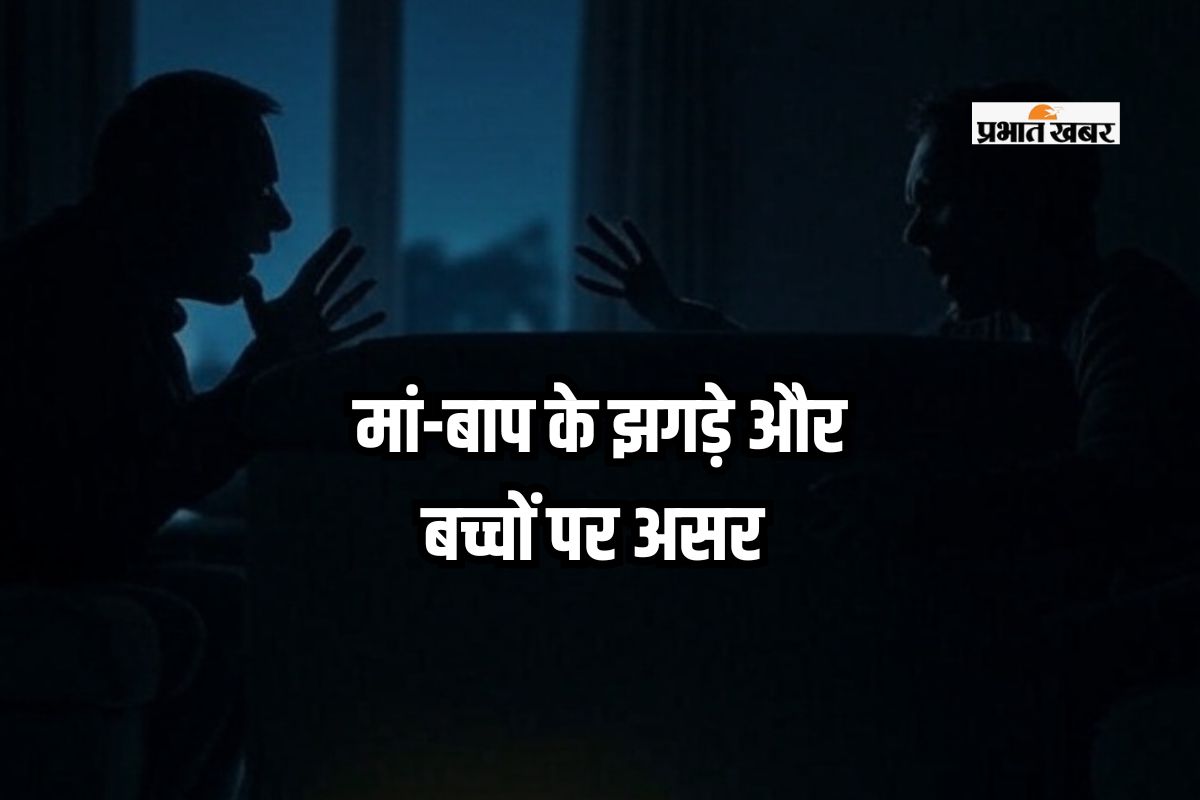Parental Quarrels: देश-दुनिया में पारिवारिक व्यवस्था के क्षय और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लगता है कि बच्चों का मसला स्नेह की बजाय माता-पिता की अदालती लड़ाई का विकट मैदान बन गया है. देखरेख करने में विफल बेटे को घर से निकालने के लिए बुजुर्ग मां-बाप के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘वसुधैव कुटुंबकम’ वाले देश में ‘एक व्यक्ति-एक परिवार’ का बढ़ता प्रचलन खतरनाक है. एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने पिछले साल के अपना फैसला पलटते हुए बच्चे के संरक्षण का अधिकार मां को सौंप दिया. जब बच्चा ग्यारह महीने का था, तब से मां-बाप के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी. तलाक के बाद बच्चे का संरक्षण मां को मिला, पर कुछ साल बाद मां ने दूसरी शादी कर पति के साथ मलेशिया में रहने का निर्णय लिया. सौतेले पिता के अनुसार ईसाई धर्म में बच्चे के धर्म परिवर्तन के बाद अदालत से बच्चे के संरक्षण का अधिकार जैविक पिता के पास वापस आ गया, पर मां ने पुनर्विचार याचिका में डॉक्टर और मनोचिकित्सक की रिपोर्ट लगाते हुए कहा कि बच्चा शुरुआत से मां के पास रहा है. अब पिता के पास रहने से उसके अंदर नकारात्मकता और अवसाद बढ़ गया है. इन नये तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने अपने पिछले साल का फैसला पलटते हुए बच्चे के संरक्षण का अधिकार मां को फिर से सौंप दिया है. पारिवारिक व्यवस्था से जुड़े इस मामले के चार संवैधानिक पहलुओं पर समझ जरूरी है.
बच्चों के संरक्षण के लिए सभी धर्मों के लिए भारत में अलग कानून हैं
पहला : सामंती और पितृसतात्मक समाज वाले ब्रिटेन में पारंपरिक तौर पर पिता का बच्चों पर अधिकार रहा है, पर कस्टडी ऑफ इन्फैंट्स एक्ट, 1839 के कानून से मां को भी बच्चों के संरक्षण का अधिकार मिला. फिर गार्जियनशिप ऑफ इन्फैंट्स एक्ट, 1886 के कानून के अनुसार मां और पिता को समान अधिकार कानूनी अधिकार मिला. साल 1925 के कानून में बच्चे के हित को सर्वोत्तम बताते हुए माता-पिता के समान कानूनी अधिकारों को स्थापित किया गया. ब्रिटिश कॉमन लॉ कानून के अनुसार भारत में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 बना. इसके अनुसार पिता के अधिकार को वरीयता मिली, पर हिंदू मेजोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 के कानून से नाबालिग बच्चे की सुरक्षा, कल्याण, विकास और संवर्धन को सर्वोच्च वरीयता मिली. तलाक के बाद बच्चों के संरक्षण के लिए सभी धर्मों के लिए भारत में अलग कानून हैं. बच्चों के हित को वरीयता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के साथ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन भी हैं.
बच्चों के संरक्षण के बारे में विधिक अस्पष्टता से बड़े पैमाने पर बढ़ रही है मुकदमेबाजी
दूसरा : औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव के लिए विधि आयोग ने 2014 में एक विचारपत्र जारी किया था. विस्तृत चर्चा के बाद केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनेक विरोधाभासी फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बच्चों के संरक्षण के बारे में विधिक अस्पष्टता से बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी बढ़ रही है. ऐसे में, स्पष्ट कानूनी व्यवस्था जरूरी है. अमेरिका और दूसरे देशों के कानूनी अपडेट से प्रेरणा लेते हुए विधि आयोग ने अनुशंसा की कि भारत में भी नाबालिग बच्चों की जॉइंट पेरेंटिंग के बारे में कानूनी प्रावधान और स्पष्टता होनी चाहिए. इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों में संसद और सरकार ने कानून में बदलाव के लिए विशेष कार्रवाई नहीं की. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन नामक एनजीओ ने 2018 में जनहित याचिका भी दायर की थी, पर सरकार द्वारा समुचित जवाब दायर न करने से 2019 से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है.
भारतीय कानून के अनुसार विदेशी बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता
तीसरा : संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती और उन्हें सिर्फ बड़ी बेंच द्वारा ही बदला जा सकता है. अनुच्छेद 137 और 145 में पुनरावलोकन के लिए बहुत सीमित आधार हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आयी, उसके आधार पर पुनरावलोकन की आड़ में पुराने फैसले को बदलने से जजों के अधिकार क्षेत्र में नयी तरह की बहस शुरू हो सकती है. इस फैसले में एक और विसंगति यह है कि जब मां दूसरे पति के साथ विदेश चली गयी, तो जैविक पिता से बच्चे की नियमित मुलाकात कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दौरान ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अन्य फैसले में कहा कि भारतीय कानून के अनुसार विदेशी बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता, भले वे रिश्तेदार ही क्यों न हों.
मां- बाप के झगड़े में बच्चों को न्यायिक विवाद से दूर रखने की जरूरत
चौथा : ब्रिटेन में 16 साल के बच्चों के मतदान के अधिकार का कानून बन रहा है. अमेरिकी कानून के अनुसार 13 साल से बड़ी उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वॉइन कर सकते हैं. भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे माता-पिता की बजाय दादा-दादी, नाना-नानी या तीसरे पक्ष के साथ रहने का भी कानूनी विकल्प दे सकते हैं. जजों के मुताबिक, मां- बाप के झगड़े में बच्चों को अदालत और न्यायिक विवाद से दूर रखने की जरूरत है. इसलिए पारिवारिक अलगाव और हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस और अदालत के सिस्टम में पिसते बच्चों के भविष्य के बारे में समाज और संसद को भी नये तरीके से सोचना होगा.
(ये लेखक के निजी विचार हैं.)