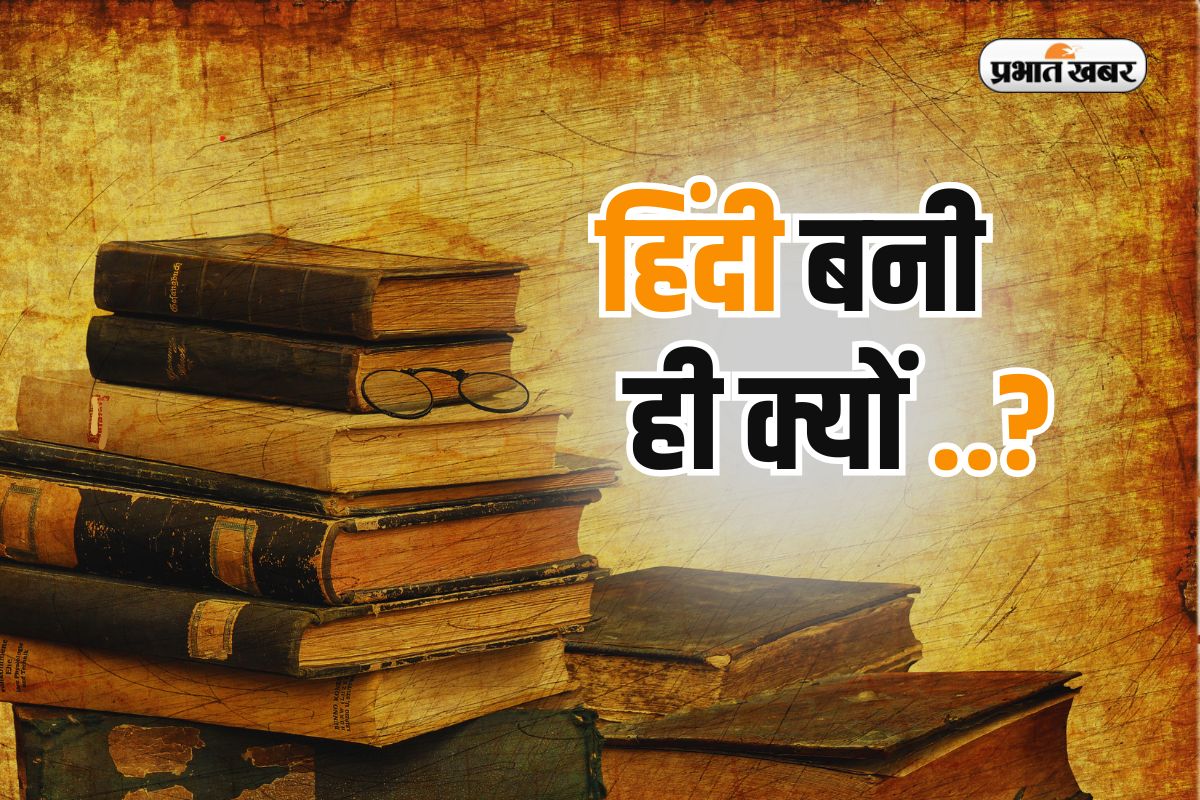Why Hindi Invented: हिंदी भारत की प्रमुख भाषा और राजभाषा है, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है. 1947 में आजादी मिलने के बाद यह अपेक्षा की गई थी कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनेगी, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे केवल “राजभाषा” के रूप में मान्यता दी. आजादी के 77 साल बाद भी हिंदी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है. दिलचस्प बात यह है कि हिंदी में कविता लिखने वाले कई कवि “राष्ट्रकवि” तो कहलाए, पर हिंदी खुद राष्ट्रभाषा न बन सकी. यह सवाल आज भी बहस का विषय है.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, “हिंदी भारत की राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी होगी.” इसका अर्थ यह है कि हिंदी केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों की भाषा है.
हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं?
अब सवाल यह पैदा होता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर “राष्ट्रभाषा” शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया है. केवल हिंदी ही नहीं, भारत में आधिकारिक तौर पर कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है. इसका कारण यह है कि भारत एक बहुभाषी देश है और संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिन्हें “अनुसूचित भाषाएं” कहा जाता है. चूंकि, हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसे “राष्ट्रभाषा” का दर्जा कभी नहीं दिया गया.
Why Hindi Invented: हिंदी बनी क्यों?
हिंदी को समझने के लिए उसके उद्भव और विकास को समझना जरूरी है. जॉर्ज ए ग्रियर्सन की पुस्तक “अ हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लैंग्वेज” और “एन्साइकलोपीडिया ब्रिटानिका” के अनुसार, हिंदी का उद्भव इंडो-आर्यन भाषा परिवार से माना जाता है, जो संस्कृत से निकली है. संस्कृत वैदिक काल (लगभग 1500-500 ईसा पूर्व) की प्रमुख भाषा थी, जिसे धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों (वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण) में इस्तेमाल किया जाता था.
डॉ भोलानाथ तिवारी की पुस्तक “भारतीय भाषाओं का इतिहास” के अनुसार, समय के साथ, संस्कृत से प्राकृत भाषाए विकसित हुईं, जो आम जनता की बोलचाल की भाषाएं थीं. ग्रियर्सन के अध्ययन और केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रकाशनों के अनुसार, प्राकृत से आगे चलकर अपभ्रंश (लगभग 6ठी से 12वीं शताब्दी) का विकास हुआ, जो हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का आधार बनी. अपभ्रंश में शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी जैसी बोलियां शामिल थीं.
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक “हिंदी साहित्य का इतिहास” के अनुसार, उत्तरी भारत में, विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्र में, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की प्रारंभिक बोलियाँ जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और भोजपुरी उभरीं. केंद्रीय हिंदी संस्थान के शोध के अनुसार, खड़ी बोली को बाद में आधुनिक हिंदी का आधार बनाया गया.
हिंदी का विकास कैसे हुआ?
सतीश चंद्रा की पुस्तक “द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया” और “द कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया” के अनुसार, 10वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम शासकों (दिल्ली सल्तनत और मुगल काल) के प्रभाव से हिंदी में फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों का समावेश हुआ. इससे हिंदुस्तानी भाषा का विकास हुआ, जो हिंदी और उर्दू का साझा रूप थी.
हजारीप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक “हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास” के अनुसार, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने हिंदी को लोकप्रिय बनाया. कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मुहम्मद जायसी जैसे कवियों ने अवधी, ब्रज और अन्य बोलियों में साहित्य रचकर हिंदी को समृद्ध किया.
नंददुलारे वाजपेयी की पुस्तक “आधुनिक हिंदी साहित्य” के अनुसार, 18वीं शताब्दी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया गया. इसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता था. “द कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया” के अनुसार, मुगल दरबारों और बाजारों में हिंदुस्तानी के रूप में इसका प्रयोग बढ़ा.
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और साहित्य अकादमी के प्रकाशनों के अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ मानकीकृत करने का प्रयास हुआ. भारतेंदु हरिश्चंद्र को “आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक” माना जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली में नाटक, कविता और निबंध लिखे.
पॉल आर ब्रास की पुस्तक “लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया” के अनुसार, हिंदी को उर्दू से अलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बढ़ा, जबकि उर्दू में फारसी-अरबी शब्दों का वर्चस्व बना रहा.
स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी
“द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया” और “गांधीज राइटिंग्स” के अनुसार, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया. महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने हिंदी को जन-जन की भाषा बनाने की वकालत की. भारत के संविधान (1949) के अनुच्छेद 343 के अनुसार, स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई.

हिंदी का सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान
हजारीप्रसाद द्विवेदी और साहित्य अकादमी के प्रकाशनों के अनुसार, भक्ति कवियों (जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास की भक्ति रचनाएं) ने हिंदी को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया. केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्ययनों के अनुसार, सूफी कवियों ने प्रेम और एकता के संदेश को लोकप्रिय बनाया.
साहित्य अकादमी और नंददुलारे वाजपेयी के कार्यों के अनुसार, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ और अन्य लेखकों ने खड़ी बोली में उपन्यास, कहानी और कविता लिखकर हिंदी को आधुनिक साहित्यिक भाषा बनाया.
मीडिया और शिक्षा में हिंदी का योगदान
“द हिंदू” और “बीबीसी हिंदी” की रिपोर्ट्स के अनुसार, 20वीं शताब्दी में हिंदी अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो और बाद में टेलीविजन ने हिंदी के प्रसार को बढ़ाया. केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रकाशनों के अनुसार, हिंदी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली प्रमुख भाषा बनी.
तकनीकी और डिजिटल युग में हिंदी का प्रभाव
“स्टैटिस्टिता” और “गूगल ट्रेंड्स” के आंकड़ों के अनुसार, 21वीं शताब्दी में इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे मंचों ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया. “द टाइम्स ऑफ इंडिया” और “बीबीसी हिंदी” की रिपोर्ट्स के अनुसार, हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स और बॉलीवुड ने भी हिंदी के प्रसार में योगदान दिया.
केंद्रीय हिंदी संस्थान और मानक हिंदी शब्दकोश के अनुसार, केंद्रीय हिंदी संस्थान और अन्य संगठनों ने हिंदी के शब्दकोश, व्याकरण और शब्दावली को मानकीकृत करने में मदद की.
जॉर्ज ए ग्रियर्सन और डॉ भोलानाथ तिवारी के अध्ययनों के अनुसार, हिंदी का विकास जनता के बीच संचार की जरूरत से हुआ. संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा थी, जबकि प्राकृत और अपभ्रंश आम लोगों की बोली थी. हिंदी ने इस अंतर को पाटा.
हिंदी का विकास क्यों और किसलिए हुआ?
“द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया” के अनुसार, भारत जैसे विविध देश में हिंदी ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को जोड़ने का काम किया. यह राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतीक बनी.
हजारीप्रसाद द्विवेदी के कार्यों के अनुसार, भक्ति और सूफी कवियों ने हिंदी को इसलिए अपनाया ताकि वे अपनी बात आम जनता तक उनकी भाषा में पहुंचा सकें.
हिंदी की इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद यह भारत की राष्ट्रभाषा न बन सकी और यही वजह है कि हिंदीभाषी हर गैर-हिंदीभाषी प्रदेश में तौहीन का शिकार होते हैं. उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है.
ये भी पढ़ें: IAS रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं? इस सवाल ने घुमा दिया अच्छे-अच्छों का दिमाग!